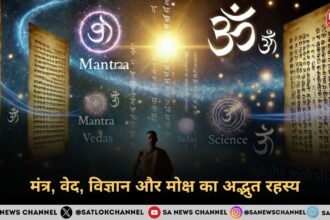हर इंसान का एक सपना होता है, अपना घर। यह सपना मिडल क्लास और गरीब तबके के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, उम्मीदों और सम्मान का प्रतीक होता है। एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे हँसते-खेलते बड़े हों, जहाँ परिवार एक साथ सुख-दुख बाँटे, और जहाँ भविष्य की नींव मजबूत हो। लेकिन इस सपने को सच करने में हजारों अड़चनें सामने आती हैं।
सबसे बड़ी तो ये कि घर गाँव में बनाए या शहर में । गाँव में जड़ें हैं, जहाँ खेती, मजदूरी या छोटा-मोटा काम जीवन का आधार है, तो शहर की चमक-धमक बच्चों की पढ़ाई, नौकरी और सामाजिक दबावों के लिए खींचती है। हालाँकि, आज के दौर में गाँवों में बढ़ते संसाधनों ने इस दौड़ को थामने का एक नया रास्ता दिखाया है। आइए, इस लेख में विस्तार से समझें कि मिडल क्लास और गरीब तबके के सपनों का घर अब गाँव में भी संभव है, और शहर की ओर भागने की जरूरत क्यों कम हो सकती है।
सपनों का बोझ और हकीकत की राह
मिडल क्लास और गरीब परिवारों के लिए घर बनाना एक भावनात्मक और आर्थिक जंग है। गाँव में रहने वाला मजदूर सोचता है कि शहर में मेहनत करूँगा, पैसा कमाऊँगा और अपने परिवार के लिए एक पक्का मकान बनाऊँगा। लेकिन शहर पहुँचते ही उसे किराए के मकानों की ऊँची कीमतें, छोटी-सी जगह और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ झेलना पड़ता है।
दूसरी ओर, मिडल क्लास परिवार महीने की तनख्वाह और लोन की किश्तों के बीच फँस जाता है। बढ़ती महंगाई, जमीन के दाम और ब्याज की दरें उनके सपनों को पीछे धकेलती हैं। फिर भी, ये परिवार हार नहीं मानते। उनके लिए घर सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि उनकी पहचान और आत्मसम्मान का हिस्सा है।
गाँव का नया रूप: एक बदलती तस्वीर
पहले गाँवों को पिछड़ा माना जाता था। न बिजली थी, न पक्की सड़कें, न अच्छे स्कूल और न ही स्वास्थ्य सुविधाएँ। लेकिन आज गाँवों का चेहरा बदल रहा है। सरकार की योजनाओं और तकनीक के प्रसार ने गाँवों को नई ताकत दी है।
- शिक्षा और तकनीक: गाँवों में स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। डिजिटल शिक्षा ने बच्चों को ऑनलाइन कोर्स और इंटरनेट के जरिए शहर जैसी सुविधाएँ दी हैं। 2025 तक ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 900 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जो युवाओं को घर बैठे स्किल सीखने का मौका दे रहा है।
- रोजगार के अवसर: ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्योग जैसे डेयरी फार्मिंग, हैंडलूम और कुटीर उद्योग फल-फूल रहे हैं। MGNREGA ने बीते वर्षों में 2.95 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जिससे गाँव में ही कमाई संभव हुई।
- बुनियादी सुविधाएँ: PMGSY के तहत पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य केंद्रों की पहुँच ने गाँवों को शहरों से जोड़ा है। मोबाइल क्लीनिक और ग्रामीण अस्पताल अब दूरदराज के इलाकों तक सेवाएँ ले जा रहे हैं।
यह बदलाव गाँवों को आत्मनिर्भर बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या शहर की ओर भागना जरूरी है, जब गाँव में ही इतने अवसर मौजूद हैं?
शहर की चकाचौंध और प्रॉपर्टी का बोझ
शहरों में सपनों का घर बनाना आसान नहीं। 2025 में शहरी संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुंबई में प्रति वर्ग फुट 21,900-22,200 रुपये और हैदराबाद में 7,300 रुपये तक पहुँच गई हैं। एक छोटे से फ्लैट के लिए भी लाखों रुपये चाहिए, जो मिडल क्लास और गरीब तबके की पहुँच से बाहर है। किराए के मकान में रहना भी महँगा सौदा है—महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और बिलों में चला जाता है। इसके अलावा, शहरों की भीड़, प्रदूषण और तनाव भरी जिंदगी सपनों को बोझ बना देती है।
दूसरी ओर, गाँव में जमीन सस्ती है। कई परिवारों के पास पैतृक जमीन होती है, जिसे वे अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ निर्माण लागत भी कम है, और सरकारी योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) आर्थिक मदद देती हैं। गाँव में घर बनाना न सिर्फ किफायती है, बल्कि यह परिवार को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है।
चुनौतियाँ जो अभी भी बाकी हैं
गाँवों में सुधार के बावजूद कुछ चुनौतियाँ बरकरार हैं। अच्छी नौकरियों के लिए अब भी शहर जाना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनियाँ और बड़े ऑफिस शहरों में ही केंद्रित हैं। इसके अलावा, सामाजिक दबाव भी एक बड़ी बाधा है। शादी के मामले में “शहर का लड़का” या “शहर की लड़की” वाली सोच ग्रामीण परिवारों को प्रभावित करती है। एक सर्वे के अनुसार, 2024 में उच्च वर्गीय परिवारों में ग्रामीण लड़कों की शादी की संभावनाएँ शहरी लड़कों की तुलना में कम मानी गईं। यह सोच परिवारों को शहर की ओर धकेलती है, भले ही वे गाँव में खुशहाल हों।
इसके अलावा, गाँवों में बड़े अस्पतालों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी अब भी है। लेकिन अगर सरकार और समाज मिलकर इन कमियों को दूर करें, तो गाँव में रहना और सपने पूरे करना आसान हो सकता है।
शहर की दौड़ क्यों कम करें?
शहर की ओर भागने की बजाय गाँव में रहने के कई फायदे हैं:
- आर्थिक बचत: शहर में घर खरीदना या किराया देना महँगा है। गाँव में कम खर्च में पक्का घर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक मिडल क्लास परिवार शहर में 50 लाख के फ्लैट के लिए लोन लेगा, लेकिन गाँव में 10-15 लाख में घर तैयार हो सकता है।
- जीवन की गुणवत्ता: गाँव में शुद्ध हवा, खुली जगह और शांति है। शहरों में प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है।
- सपनों का सच: गाँव में बढ़ते संसाधन और सरकारी सहायता ने घर बनाने को हकीकत में बदल दिया है। PMAY-G के तहत 2021-22 में 5,854 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो ग्रामीण परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है।
- सांस्कृतिक जुड़ाव: गाँव में रहने से परिवार अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा रहता है, जो शहर की भागदौड़ में खो जाती है।
कोविड के बाद गाँवों की ओर शिफ्ट: शोध और सबूत
- लॉकडाउन और रिवर्स माइग्रेशन:
2020 में भारत में लगे सख्त लॉकडाउन के दौरान, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खत्म होने और अनिश्चितता बढ़ने के कारण करीब 2-3 करोड़ प्रवासी मजदूर अपने गाँवों की ओर लौट गए। एक अध्ययन, “Urban to Rural COVID-19 Progression in India” (Sahoo et al., 2022), में बताया गया कि मई से सितंबर 2020 के बीच शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 का प्रसार बढ़ा, जो प्रवासियों के वापसी से जुड़ा था। यह रिवर्स माइग्रेशन अस्थायी था, लेकिन इसने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू की। - ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
“Migration and Its Impact on the Rural Economy During Covid-19” (Anand, 2023) में पाया गया कि लौटे हुए प्रवासियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सहारा दिया, खासकर कृषि क्षेत्र में। कई लोग शहरों में अनिश्चितता और महँगी प्रॉपर्टी कीमतों (जैसे मुंबई में 2025 में प्रति वर्ग फुट 22,000 रुपये) के कारण गाँवों में रहने पर विचार करने लगे। हालाँकि, यह शिफ्ट अस्थायी थी, क्योंकि रोजगार की कमी ने कई लोगों को फिर से शहरों की ओर लौटने के लिए मजबूर किया। - लंबी अवधि का रुझान:
“Internal Migration During COVID-19 Pandemic” (Journal of Rural Development, 2022) में यह तर्क दिया गया कि कोविड के बाद कुछ लोग गाँवों में स्थायी रूप से बसने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर वे जो डिजिटल नौकरियों या दूरस्थ कार्य (remote work) से जुड़े हैं। 2025 तक ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 900 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जो गाँवों में रहकर काम करने की संभावना को बढ़ाता है। लेकिन यह रुझान मध्यम वर्ग या शिक्षित लोगों तक सीमित है, न कि बड़े पैमाने पर गरीब तबके तक। - सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ:
“The Plight of Migrants During COVID-19” (Humanities and Social Sciences Communications, 2021) में उल्लेख किया गया कि गाँवों में रोजगार के सीमित अवसर और सामाजिक दबाव (जैसे शादी के लिए “शहर का लड़का” पसंद करना) लोगों को फिर से शहरों की ओर खींचते हैं। इसलिए, गाँवों में स्थायी शिफ्टिंग सीमित रही।
क्या लोग स्थायी रूप से गाँवों में शिफ्ट हो रहे हैं?
- कुछ हद तक , हाँ : शिक्षित मध्यम वर्ग, जो डिजिटल नौकरियाँ कर सकता है, और कुछ परिवार जो शहरी जीवन की महँगाई से बचना चाहते हैं, गाँवों में शिफ्ट हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों (PMGSY), बिजली और इंटरनेट की बढ़ती सुविधाएँ इसे संभव बना रही हैं।
- बड़े पैमाने पर , नहीं : गरीब और मजदूर वर्ग के लिए गाँवों में रोजगार की कमी और बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत उन्हें शहरों की ओर वापस ले जाती है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 63.64% आबादी अभी भी गाँवों में रहती है, लेकिन शहरीकरण का रुझान जारी है।
एक नई सोच की जरूरत
गाँवों में बढ़ते संसाधन इस बात का सबूत हैं कि अब शहर ही सबकुछ नहीं है। लेकिन इस बदलाव को पूरी तरह अपनाने के लिए समाज और सरकार दोनों को आगे आना होगा। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और नौकरी के अवसर लाने होंगे।
साथ ही, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। गाँव में घर होना या वहाँ रहना कमतर नहीं है—यह आत्मनिर्भरता, गर्व और जड़ों से जुड़ाव की निशानी है। अगर “शहर का लड़का” वाली मानसिकता टूटे और गाँव में ही बेहतर भविष्य की नींव रखी जाए, तो मिडल क्लास और गरीब तबके के लिए सपनों का घर बनाना आसान हो जाएगा।
अपनी आवश्यकता देखिए, दूसरे का घर नहीं
संत रामपाल जी की शिक्षाएँ इस लेख के संदर्भ में एक गहरा और प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। वे सादगी, ईमानदारी और आध्यात्मिकता को जीवन का आधार मानते हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संपत्ति का पीछा करने की बजाय हमें आध्यात्मिक समृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। एक वाणी के माध्यम से वो बताते हैं कि , “काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो,” । ये इस बात को रेखांकित करता है कि यह शरीर ही जब हमारा अपना नहीं है तो ये धन संपत्ति कहाँ से हो सकती हैं ।
संत रामपाल जी घर बनाने में भव्यता की बजाय मध्यम और सुविधाजनक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। वे डोवरी सिस्टम और भव्य रीति-रिवाजों का विरोध करते हैं, जो गरीब और मिडल क्लास परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालते हैं।
उनकी Dowry-Free India Campaign इस बात का प्रमाण है कि वे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके सभी आश्रमों में सभी को मुफ्त भोजन देना और बराबर सुविधाएँ देना, सादगी और मानवता का एक जीवंत उदाहरण है।
कबीर साहेब जी की वाणी :
“कहा चुनावै मेड़िया, लम्बी भीत उसारि ।
घर तो साढ़े तीन हाथ, घना तो पौने चारि” ।।
एक गहरा संदेश देती है। संत रामपाल जी महाराज इसका अर्थ बताते हैं कि लोग बड़े-बड़े सपने देखते हैं और ऊँची दीवारें (“लम्बी भीत”) बनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन वास्तव में एक इंसान को जीने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है।
यहाँ “साढ़े तीन हाथ” (लगभग 5-6 फीट) और “पौने चारि” (लगभग 6-7 फीट) से तात्पर्य उस न्यूनतम स्थान से है, जो एक व्यक्ति को सोने या रहने के लिए चाहिए। भावार्थ यह है कि भव्य और विशाल घर बनाने की चाहत व्यर्थ है, क्योंकि इंसान की मूलभूत आवश्यकता सीमित होती है। यह एक व्यावहारिक और दार्शनिक संदेश है कि हमें अपनी जरूरतों के अनुसार ही घर बनाना चाहिए, न कि दिखावे या लालच में पड़कर अनावश्यक भव्यता का पीछा करना चाहिए।
गाँव और शहर की अगर मगर से इतर ये एक ऐसा संदेश हैं कि अगर इसे अपना लिया जाए तो ये प्रॉपर्टी की दौड़ भी मिट जाएगी और हर व्यक्ति के पास अपना गुजर बसर करने और भगवान भी भक्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे । अधिक जानकारी के लिए उनकी पुस्तक “जीने की राह” निशुल्क मँगवाई जा सकती है ।
“एक तरफ आपके सपनों का घर, फिर गाँव-शहर की अगर-मगर” लाखों लोगों की जिंदगी का सच है। गाँव अब पहले जैसे नहीं रहे—यहाँ संसाधन बढ़े हैं, सुविधाएँ आई हैं और आत्मनिर्भरता की राह खुली है। शहर की महँगी प्रॉपर्टी और तनाव भरी जिंदगी की बजाय गाँव में सस्ता, सुविधाजनक और संतोषजनक घर बनाया जा सकता है। यह समय है किहम अपनी जरूरतों को पहचानें और आवश्यकतानुसार ही खर्च करके घर बनाए न कि किसी दिखावे के लिए।
गाँव-शहर की अगर-मगर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- संत रामपाल जी घर बनाने के लिए क्या सलाह देते हैं?
संत रामपाल जी सादगी और आध्यात्मिकता पर जोर देते हैं। वे भव्य और महँगे घरों की बजाय मध्यम, सुविधाजनक और किफायती घर बनाने की सलाह देते हैं, ताकि आर्थिक बोझ न बढ़े और जीवन शांतिपूर्ण रहे। - गाँव में घर बनाना शहर के मुकाबले क्यों बेहतर है?
गाँव में जमीन सस्ती है, निर्माण लागत कम है, और पैतृक जमीन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें—like मुंबई में 22,000 रुपये प्रति वर्ग फुट—मिडल क्लास के लिए सिर्फ एक सपना भर हैं। - क्या गाँव में संसाधन अब शहर जैसे हो गए हैं?
हाँ, काफी हद तक। PMGSY ने सड़कें बनाईं, MGNREGA ने रोजगार दिया, और 2025 तक ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता 900 मिलियन होने का अनुमान है। हालाँकि, बड़े अस्पताल और शिक्षण व्यवस्थाएँ अभी भी चुनौती हैं। - शहर की दौड़ छोड़ने से मिडल क्लास को क्या फायदा होगा?
आर्थिक बचत होगी, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, और परिवार अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। गाँव में सस्ता घर बनाना और शांत जीवन जीना शहर की तनावपूर्ण जिंदगी से बेहतर विकल्प है। - सामाजिक दबाव जैसे शादी में “शहर का लड़का” वाली सोच को कैसे तोड़ा जाए?
गाँवों में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने से यह सोच बदलेगी। संत रामपाल जी की शिक्षाएँ भी दहेज और सामाजिक दिखावे का विरोध करती हैं, जो इस मानसिकता को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। - क्या सरकारी योजनाएँ वास्तव में गाँवों में घर बनाने में मदद करती हैं?
हाँ, PMAY-G जैसी योजनाएँ आर्थिक सहायता देती हैं। 2021-22 में 5,854 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिससे लाखों परिवारों को पक्के घर मिले। लेकिन कागजी कार्रवाई और जागरूकता की कमी अभी भी बाधा है।